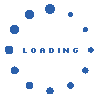नमस्कार, गणमान्य अतिथियों, देवियो और सज्जनो!
केरल में विश्व आयुर्वेद महोत्सव के अंतर्गत विज़न कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है।
केरल परम्परागत आयुर्वेद का मुख्य केंद्र है। ऐसा महज़ इसलिए नहीं है कि राज्य में आयुर्वेद की लंबी, अविच्छिन्न परिपाटी रही है, बल्कि इसलिए भी है कि यहां की प्रामाणिक औषधिय़ा एवं चिकित्सा पद्धतियां विश्व प्रसिद्ध हैं, और अब विशाल, तेज़ी से बढ़ते आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के तंत्र के कारण ऐसा है।
मुझे बताया गया है कि यह पांच दिवसीय विश्व आयुर्वेद महोत्सव आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं पर सहभागिता एवं हिस्सेदारी के दृष्टिकोण से अत्युत्तम रहा है।
यह जानना सुखद है कि विभिन्न देशों से बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि आयुर्वेद महोत्सव में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं आश्वस्त हूं कि महोत्सव में उनकी भागीदारी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करेगी।
भारत में ऋषियों एवं संन्यासियों की लंबी परम्परा है जिन्होंने स्वयं अपनी स्वदेशी स्वास्थ्य सेवाओं का तंत्र विकसित किया, जैसे आयुर्वेद, योग एवं सिद्ध पद्धतियां।
समय बीतने के साथ हमने विभिन्न सभ्यताओं से वार्तालाप किया और दूसरी चिकित्सा पद्धतियों का समावेश भी किया।
यह सभी पद्धतियां “सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयः” यानी 'सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें' के दर्शन पर आधारित थीं।
आयुर्वेद को सामान्यतया जीवन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है- 'आयु' यानी जीवन एवं 'वेद' यानी विज्ञान। सुश्रुत ने स्वास्थ्य की परिभाषा यह दी हैः
समदोषः समाग्निश्च समधातु मलःक्रियाः।
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनः स्वस्थइतिअभिधीयते॥
अर्थात यदि सभी त्रिदोष अथवा जैव ऊर्जा एवं अग्नि अथवा चयापचय की प्रक्रिया संतुलित रहती है, और यथोचित मलोत्सर्जन होता है तब स्वास्थ्य संतुलित रहता है। जब आत्मा, इंद्रियां, मन या बुद्धि आंतरिक शांति के साथ तारतम्य में होते हैं- सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है।
इस परिभाषा की तुलना विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा से कीजिएः स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्तरों पर पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को कहा जाता है- न कि महज़ रोग या दौर्बल्य की अनुपस्थिति को। लिहाज़ा आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद के सिद्धांत विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दी गई परिभाषा के साथ लयबद्ध हैं।
स्वास्थ्य पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को कहा जाता है एवं रोग रहित होने को नहीं।
आज आयुर्वेद के विशद एवं समग्र दृष्टिकोण के कारण इसकी वैश्विक प्रासंगिकता है।
आयुर्वेद के मतानुसार 'दिनचर्या' जीवन में शांति एवं समरसता लाने में सहायता प्रदान करती है। आयुर्वेदिक चर्या मनुष्य के जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य संवर्द्धन, मानसिक एवं शारीरिक, को ध्यान में रख कर बनाई गई है।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कौन सी चुनौतियां हैं जो विश्व के सामने हैं? गैर संक्रामक रोग, जीवनचर्या से जुड़े रोग जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एवं कर्कटार्बुद (कैंसर) सबसे बड़ी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बन गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार ग़ैर संक्रामक रोगों से प्रतिवर्ष 38 मिलियन लोग मरते हैं, इनमें से 28 मिलियन निम्न एवं मध्य आय वर्ग वाले देशों में होती हैं। आयुर्वेद इनके प्रबंधन हेतु समाधान प्रस्तुत करता है।
संतों एवं संन्यासियों की लंबी परम्परा, जिसने स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद, योग एवं सिद्ध विज्ञान जैसी पद्धतियों की रचना की, प्रकृति से सामंजस्यपूर्ण संबंधों में विश्वास करती है।
यह सारी पद्धतियां संतुलन का प्रयास करती हैं एवं पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार एवं जड़ी बूटियों के दीर्घकालिक उपचार से स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं।
दुर्भाग्यवश कई वजहों से आयुर्वेद की वास्तविक सामर्थ्य का प्रयोग नहीं हो पाया है। अपर्याप्त वैज्ञानिक अनुसंधान और मानक एवं गुणवत्ता संबंधी चिंताएं इनमें प्रमुख कारण हैं।
यदि इन विषयों पर ठीक से ध्यान दिया जाए, मैं आश्वस्त हूं कि आयुर्वेद से कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। भारत विश्व को सर्वांगीण स्वास्थ्य रक्षा सरलता से मुहैया कराने के मामले में नेतृत्व प्रदान कर सकता है।
इन विषयों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, एवं हम क्या कर रहे हैं?
हमारी सरकार आयुर्वेद एवं परम्परागत औषधियों को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्णतः समर्पित है। इस सरकार के बनते ही आयुष विभाग को भारत सरकार के एक पूर्ण मंत्रालय में तब्दील कर दिया गया था।
आयुष औषधीय पद्धति का उन्नयन करने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत लागत कुशल आयुष सेवाएं, शैक्षिक संस्थाओं का सशक्तिकरण, आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी और होम्योपैथी दवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण एवं कच्चे माल की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। आयुष औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर नियमन के प्रावधानों में संशोधन लाने एवं नियमन के ढांचे को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
दवाओं के केंद्रीय मानक नियंत्रण संगठन में आयुष दवाओं का ढांचा खड़ा किया जा रहा है, भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण एवं गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राज्यों की वित्तीय सहायता में विस्तार- वे अहम क़दम हैं जो जारी हैं।
योग विशेषज्ञों का कौशल एवं ज्ञान की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए गत वर्ष 22 जून को समग्र स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान योग पेशेवरों के स्वैच्छिक प्रमाणन की योजना प्रारंभ की गई थी।
आयुर्वेद एवं औषधियों की अन्य भारतीय पद्धतियों के बारे में हमारी नीति विश्व स्वास्थ्य संगठन की पारम्परिक दवा रणनीति 2014-2023 के अनुरूप है, जिसको संगठन के 192 देशों द्वारा क्रियान्वयन हेतु विश्व स्वास्थ्य असेंबली के दौरान अपनाया गया था।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रणनीति में स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं व्यक्ति केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पारंपरिक एवं संपूरक औषधियों के योगदान का प्रयोग करने की विधिया हैं।
स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, अतएव, हमें- "पूर्व के श्रेष्ठतम का पश्चिम के श्रेष्ठतम से मेल करना चाहिए।"
औषधियों की आधुनिक पद्धतियों में सशक्त एवं प्रभावी नैदानिक तरीक़े हैं जिनसे हमें रोगों की शीघ्र पहचान करने में मदद मिलती है। स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक के प्रयोग में देखभाल के रास्ते की बाधाएं कम करने और रोग के स्वरूप के प्रति हमारी समझ विकसित करने की सामर्थ्य है।
यद्यपि हमें इसके इतर देखने की आवश्यकता भी है। हमें स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने एवं बेहतर स्वास्थ्य की तलाश के साथ शारीरिक एवं मानसिक तंदुरुस्ती के संयोजन से इतर देखने की भी ज़रूरत है।
उपचार की बढ़ती क़ीमत एवं दवाओं के दुष्प्रभाव ने चिकित्सा विशेषज्ञों को औषधियों की पारंपरिक पद्धतियों के क्षितिज का विस्तार करने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है। हम अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में शोध के नियमन एवं स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तम उत्पादों, तौर तरीक़ो एवं चिकित्सकों के समेकन के माध्यम से पारंपरिक औषधियों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं।
हमारा प्रयास है कि आयुर्वेद एवं अन्य आयुष पद्धतियों की वास्तविक सामर्थ्य का प्रयोग लोगों को सुरक्षात्मक, प्रोत्साहक एवं संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में किया जाए।
हम आयुर्वेद एवं अन्य उपचारात्मक पद्धतियों का प्रयोग उनके स्वभाव एवं सूक्ष्मता के अनुरूप बढ़ाएंगे एवं संपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन में सहायता करेंगे। युवा उद्यमी, जो किसी स्टार्टअप की योजना बना रहे हों, वे समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र की योजना के संदर्भ में एक ओर जहां हम आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता एवं समकालीन प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करते हैं, इन पद्धतियों की वस्तुस्थिति एवं चुनौतियों पर चिंतन करना भी महत्वपूर्ण है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक औषधियां कई लोगों के लिए वहन करने योग्य हैं। यह सबके लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध है, अपनी प्रभावोत्पादकता एवं हिफाज़त के लिए समय द्वारा परीक्षित है। सबसे अहम है कि यह उन समुदायों की संस्कृति एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप है जहां यह पैदा होती हैं। विकासशील देशों के कई हिस्सों में निर्धनों की वित्तीय एवं भौतिक पहुंच के दृष्टिकोण से परम्परागत चिकित्सा पद्धतियां अकेला संसाधन हैं।
इसलिए यह और अधिक महत्वपूर्ण है कि हम इन पद्धतियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
यहां आयुर्वेद से जुड़े समस्त महानुभाव इस पर सहमत होंगे कि आयुर्वेद के सुरक्षा,
फलोत्पादकता, गुणवत्ता, पहुंच जैसे पक्षों एवं हमारे पारम्परिक औषधीय ज्ञान का तर्कसंगत उपयोग आदि मामलों पर ध्यान देना हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
मैं जानता हूं कि चीन में पारम्परिक चीनी दवाओं के सुरक्षित उपयोग पर नीतियों के विकास एवं नियमन हेतु बड़े प्रयास हो रहे हैं, जिनसे संपूरक एवं वैकल्पिक औषधियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा जुड़ा है।
हम दूसरे देशों के अनुभव से सीखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आयुर्वेद एवं दूसरी भारतीय पद्धतियां लोकप्रिय एवं प्रसारित हों।
मुझे बताया गया है कि फरवरी 2013 में पारम्परिक औषधियों पर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों द्वारा स्वीकृत दिल्ली घोषणापत्र, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति द्वारा स्पष्ट किया गया था, में सदस्य देशों द्वारा पारम्परिक औषधियों के विकास संबंधी गतिविधियों हेतु सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की गई है।
मैं आशा करता हूं कि दिल्ली घोषणापत्र के अनुच्छेदों के विधिवत क्रियान्वयन से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर आयुर्वेद समेत पारम्परिक औषधियों के सुनियोजित विकास में मदद मिलेगी। हम आयुर्वेद एवं अन्य आयुष पद्धतियों में प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विनिमय कार्यक्रमों हेतु अपने संस्थानों को निर्दिष्ट केंद्रों के तौर पर प्रस्तावित करते हैं।
इन क्षेत्रों में हमारा नेतृत्व केवल निरंतर प्रयासों से बना रह सकता है जिनमें उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्रदान की जाए एवं प्रतिस्पर्धी व्यवसायी पैदा किए जाएं।
देवियो एवं सज्जनो, जैसा कि आप जानते हैं, भारत में आयुर्वेद एवं योग का लंबा इतिहास एवं संपन्न धरोहर है। आयुर्वेदिक ज्ञान का बहुसांस्कृतिक उद्गम शास्त्रों में उद्घाटित है। चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता दोनों ही वैद्य़ों से औषधीय पौधों हेतु चरवाहों, बहेलियों एवं वनवासियों की मदद लेने का अनुरोध करती हैं।
आयुर्वेद के सिद्धांतों की रचना हेतु आयोजित विद्वज्जनों की एक सभा में मध्य एशिया से एक वैद्य के सम्मिलित होने और योगदान देने की बात चरक संहिता से पता चलती है।
तीन महत्वपूर्ण शास्त्रीय इबारतें बुद्ध की नैतिक शिक्षाओं पर बल देती हैं। वाग्भट्ट, जिसको आयुर्वेद के एक शास्त्रीय ग्रंथ अष्टांग हृदयम् का रचयिता कहा जाता है, बौद्ध था।
इससे सिद्ध होता है कि यह परम्पराएं स्थानीय स्तर पर एवं विभिन्न संस्कृतियों के मध्य ज्ञान साझा करने से विकसित हुई हैं। उन्होंने इसको सर्वाधिक विनीत भाव रखने वालों से एवं गुप्तज्ञान वालों से सीखा है।
हम इस कोशिश को जारी रखेंगे। हम अपनी पद्धतियों के ज्ञान को विश्व से साझा करेंगे, और दूसरी पद्धतियों से सीखने की अपनी परम्परा को सम्पन्न बनाते रहेंगे।
विश्व आयुर्वेद सम्मेलन इसी दृष्टिकोण को आगे ले जाता है।
मैं विश्व आयुर्वेद महोत्सव एवं विज़न कॉन्क्लेव की सर्वोच्च सफलता की कामना करता हूं। मेरा विश्वास है कि महोत्सव में होने वाला विमर्श आयुर्वेद के वैश्विक स्थापन के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देगा।
मैं अपनी बात आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदयम् के शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।
व्याधियों से पीड़ित एवं दुखों से संतप्त निर्धनों की सहायता करनी चाहिए। यहां तक कि कीटों एवं चींटियों से भी करुणापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, जैसा स्वयं के प्रति किया जाता है।
यह आयुर्वेद की मार्गदर्शक विचारधारा है। आइए हम सब इसको अपनी मार्गदर्शक विचारधारा बनाएं।
धन्यवाद।